5 Legal Rights Every Indian Citizen Must Know – Protect Yourself with the Law
Legel rights of Indian citizens
भारतीय नागरिकों के 5 महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार
मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुई हो और आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस अधिकारी द्वारा आपका FIR नही लिखा जाता है। ऐसी स्थिति में आपके क्या अधिकार है ? या क्या कोई व्यक्ति जो किसी घटना में गिरफ्तार है उसको किसी वकील से मिलने का अधिकार है? आज हम इस लेख में ऐसे ही 5 महत्वपूर्ण अधिकारों की चर्चा करेंगे जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को जानना आवश्यक है।आइये आज के इस लेख को शुरू करते है!
1.पुलिस FIR लिखने से मना नही कर सकती-
कानूनी प्रावधान-
भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-154 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके साथ कोई घटना हुई हो पुलिस स्टेशन जाकर FIR (First Information Report) दर्ज करा सकता है, पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से मना नही किया जा सकता।
कैसे लागू होता है?
यदि किसी पुलिस द्वारा FIR लिखने से मना किया जाता है तो उसकी शिकायत एसपी (Superintendent of Police) या न्यायिक मजिस्ट्रेट (Judicial magistrate) के पास करें।
उदाहरण-
अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ या किसी पुरुष या महिला के साथ मार-पीट की घटना हुई हो और पुलिस शिकायत दर्ज नही करती है तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा सकती है।
2. जब तक किसी का अपराध साबित नही हो जाए, कोई अपराधी नही होता-
कानूनी प्रावधान-
अंग्रेजी में एक कथन है- “Innocent until proven guilty ” अर्थात दोषी साबित होने तक निर्दोष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम -1872 (IEA-1872) के तहत यदि किसी व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगता है तो जब तक न्यायालय में सबूतों एवं गवाहों के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा।
कैसे लागू होता है?
अभियोजन पक्ष को साबित आरोप साबित करना होगा। (अभियोजन पक्ष यानि- शिकायतकर्ता, सरकारी वकील, पुलिस, गवाहान)। पर्याप्त गवाह एवं सबूत के अभाव में या न होने पर आरोपी को दोषमुक्त कर रिहा किया जा सकता है।
उदाहरण-
यदि किसी व्यक्ति पर हत्या या बलात्कार का आरोप लगता है और सबूत और गवाह से साबित नही होता है तो उसको न्यायालय दोषी नहीं मानती है।
3. गिरफ्तार व्यक्ति को वकील/अधिवक्ता से मिलने का अधिकार-
कानूनी प्रावधान-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-22(1) व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-41D के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे वकील से मिलने की अनुमति है।
कैसे लागू होता है?
पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति अथवा आरोपी से वकील/अधिवक्ता से मिलने से नहीं रोक सकती एवं गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने परिवार जन व दोस्तों को गिरफ्तार होने की सूचना देने का अधिकार है।
उदाहरण-
यदि कोई व्यक्ति चोरी या धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो वह तुरन्त वकील से मिल सकता है।
4. महिलाओं को रात में गिरफ्तार न करने का अधिकार-
कानूनी प्रावधान-
भारत की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा-46(4) व दिलीप के. बसु बनाम राज्य सरकार के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का कथन के अनुसार किसी भी महिला को रात में सूर्यास्त के बाद से लेकर सूर्योदय के पहले तक गिरफ्तार नही किया जा सकता।
किसी विशेष परिस्थिति में जैसे- गंभीर अपराध,फरार होने की कोशिश कर रही हो या किसी अपराध स्थल पर पकड़ी गई हो तो गिरफ्तारी आवश्यक होने पर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के साथ महिला पुलिस अधिकारी का रहना ज़रूरी है।
कैसे लागू होता है?
महिला को गिरफ्तार करने की स्थिति में वह सवाल पूंछ सकती है कि क्या किसी मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति है? और महिला पुलिस का होना आवश्यक है।
अगर उपरोक्त दोनों न होने पर भी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला उच्च अधिकारी जैसे SP, DSP को शिकायत, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय/राज्य महिला आयोग में शिकायत एवं जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है जिसमें प्रमुख धाराएं- IPC की धारा 166- सरकारी अधिकारी द्वारा कानून उल्लंघन, IPC की धारा 342- गैर कानूनी रूप से किसी को कैद रखना, IPC की धारा 354- महिला के सम्मान के खिलाफ कार्य करने के आधार पर संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया जा सकता है ।
5. मेडिकल एमरजेंसी में इलाज का अधिकार-
कानूनी प्रावधान-
अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य का अधिकार भी माना है अर्थात एमरजेंसी में इलाज पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
क्लिनिकल स्टैबलिशमेंट अधिनियम (2010) सभी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल को प्राथमिक चिकित्सा देना अनिवार्य। किसी की आर्थिक स्थिति देखकर या पहचान के आधार पर इलाज करना गैर कानूनी एवं दंडनीय है।
परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (1989) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कथन किया कि कोई भी अस्पताल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल किसी भी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का इलाज करने से मना नही कर सकता।
IPC की धारा 304A व 336-338- किसी चिकित्सक (डॉक्टर) या अस्पताल द्वारा मरीज के एमरजेंसी में इलाज न देने या मना करने पर मरीज़ की मृत्यु हो जाती है तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द करना एवं जेल की सज़ा भी हो सकती है।
कैसे लागू होता है?
कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल निम्न इमरजेंसी में मरीज का इलाज करने से मना नही कर सकता है- सड़क दुर्घटना, गर्भवती महिलाओं का इलाज, हार्टअटैक, ब्रेन स्ट्रोक, गंभीर रूप से जलने पर, ब्लड लॉस, गंभीर चोट, सांस की तकलीफ, लाइफ सपोर्ट, सर्पदंश या विषैले जानवर के काटने पर, कोरोना जैसी महामारी पर।
अस्पताल द्वारा इलाज न करने पर अनुच्छेद 21,क्लिनिकल स्टैबलिशमेंट अधिनियम (2010), IPC की धारा 304A व 336-338 तथा सर्वोच्च न्यायालय के फैसलो का हवाला दें। मरीज की वीडियो रिकार्डिंग करें और अस्पताल से इलाज न करने पर लिखित में कारण मांगे।
फिर भी अस्पताल द्वारा इलाज न करने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नं- 1076, एम्बुलेंस सेवा नं-108, महिला हेल्पलाइन नं-1191, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नं- 1800-11-4000 या राज्य स्वास्थ्य विभाग के नंबर(प्रत्येक राज्य का अलग अलग, विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध) पर डायल करें।
साथ ही CMO, DHMO, मानवाधिकार आयोग, राज्य स्वास्थ्य विभाग में शिकायत करें। कंज्यूमर कोर्ट में केस दाखिल करे,एवं न्यायालय में लोकहित याचिका (PIL) भी दाखिल कर सकते हैं।
उदाहरण-
यदि किसी महिला की प्रसूति का मामला हो और अस्पताल या चिकित्सक फीस जमा न हो पाने की स्थिति में इलाज नहीं करते है तो अस्पताल प्रशासन का लाइसेंस रद्द एवं सज़ा हो सकती है।
निष्कर्ष:
आज के इस लेख में हम लोगो ने 5 प्रमुख भारतीय नागरिक अधिकारों के बारें में जाना। आशा करता हूं भविष्य में कभी आपके किसी प्रकार के अधिकार का हनन होने पर आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करेंगे।
इसी प्रकार के अन्य प्रमुख नागरिक अधिकारों को हम आने वाले अन्य लेखो में जानेंगे।
धन्यवाद! इसी प्रकार के कानूनी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.judiciaryofindia.com पर बने रहें।
Share this content:



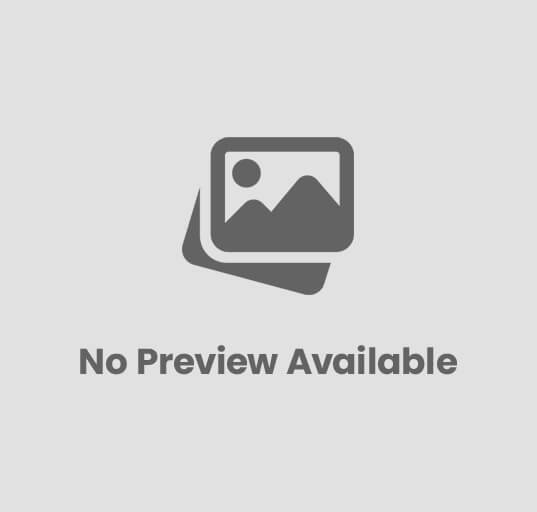







Post Comment